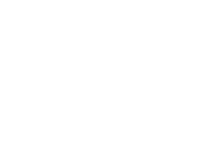

2025-08-24 16:24:47
देश में इस समय SIR, वोटर लिस्ट पर मचे सियासी शोर की आड़ में चुपके से एक खिचड़ी पक रही है। ‘भाषाई अस्मिता’ के नाम पर एक बार फिर बांटने की कोशिश हो रही है। पश्चिम बंगाल इस बार प्रयोगशाला बन रहा है और ममता बनर्जी इसकी अगुवा। 2026 के चुनावों से पहले किया जा रहा यह प्रयोग बंगाल में अशांति के बीज बो सकता है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याओं और अत्याचार जैसी घटनाओं को भड़काने में आग में घी का काम कर सकता है। ममता बनर्जी भले ही इसे भाजपा शासित राज्यों में बांग्लाभाषियों के कथित उत्पीड़न और बंगाली अस्मिता से जोड़ने की कोशिश कर रही हों लेकिन उनके दावे की हककीत, ऐसे अभियानों के पीछे की राजनीतिक मंशा और संभावित परिणामों पर विचार करना बेहद जरूरी है। भाषा के नाम पर बांटने की चाल से पार होगी चुनावी वैतरणी? दरअसल पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ममता बनर्जी द्वारा साल भर पहले ही बंगाली भाषा कार्ड को हथियार क्यों बनाया है उसके पीछे की मंशा समझना मुश्किल नहीं। ममता बनर्जी की बंगाली अस्मिता पर आधारित मुहिम अब भाषा से आगे बढ़कर सिनेमा तक पहुंच गई है। नेताओं को सिर्फ़ बंगाली में भाषण देने के आदेश के बाद तृणमूल कांग्रेस सरकार ने आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल के सभी सिनेमाघरों में प्राइम टाइम के दौरान कम से कम एक बंगाली फिल्म अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इस अभियान से स्पष्ट है कि ममता बनर्जी भाषा के नाम पर अतिवाद और बांटने की चाल को चुनावी वैतरणी पार करने में बड़ा हथियार मान रही हैं। लेकिन गंभीर सवाल यह है कि इसके परिणाम क्या होंगे? इसे समझने के लिए ममता के बयानों से इतर और असल आंकड़ों पर गौर करना होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा इस अभियान के पीछे बांग्लाभाषियों के कथित उत्पीड़न को बाताया गया। ऐसे में ममता बनर्जी के इन दावों की हकीकत जानने के लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि क्या वाकई बंगाल के लोगों का भाषा के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है या यह अभियान सिर्फ बांटने का प्रयोगभर है? ममता बनर्जी के दावे और हकीकत ऊपर उठाए गए सवालों के जवाब तक पंहुचने से पहले बंगाली भाषा की देश में स्थिति को जानना जरूरी है। 2011 की जनगढ़ना के मुताबिक भारत में बंगाली मातृभाषा (first) बोलने वालों की संख्या लगभग 97,237,669 है, जो कुल जनसंख्या का 8.03% है। बंगाली भाषा को केवल मातृभाषा न मानकर यदि इसे किसी अन्य क्रम में बोलने वालों को भी शामिल किया जाए तो कुल संख्या बढ़कर करीब 107.47 लाख (10.75 करोड़) हो जाती है। इस तरह बंगाली हिन्दी के बाद भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इतना ही नहीं इंटरनेट पर भी बंगाली भाषा की पहुंच बढ़ी है। KPMG-Nielsen के डेटा के अनुसार, 2021 तक इंटरनेट उपयोग करने वालों में 46% बंगाली भाषा उपयोगकर्ता हो सकते हैं। सत्य से कोसों दूर नरेटिव गढ़ने की कोशिश बात करें राज्यवार बंगाली भाषा की स्थिति का तो बंगाल के अलावा अन्य राज्यों में भी बंगाली भाषा बोली जाती है। असम की बराक वैली में 2.93 मिलियन लोग बंगाली भाषा बोलते हैं ये आंकड़ा वहां की जनसंख्या का 80.84% है। ब्रह्मपुत्र घाटी में 6.09 मिलियन लोग बंगाली भाषा बोलते हैं जो कि कुल जनसंख्या का 22.09% है। त्रिपुरा में 2.41 मिलियन लोग बंगाली बोलते हैं जो वहां कि जनसंख्या का 67.73% है। अंडमान व निकोबार में 1.08 लाख लोग बंगाली लिखते व बोलते हैं जो कि वहां कि जनसंख्या का 28.49 प्रतिशत हिसा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी बंगाली भाषा बोलने वालों की संख्या अच्छी खासी है, लगभग 2.16 लाख लोग यहां गर्व से बंगाली बोलते हैं। यहां के कई इलाकों में बंगाली महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत है, खासकर चित्तरंजन पार्क जैसी बस्तियों में जो बंगाली संस्कृति के प्रमुख केंद्र हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो आंकड़े दिए गए हैं उन सभी जगहों पर बीजेपी की ही सरकार है- असम, त्रिपुरा, दिल्ली में और अंडमान व निकोबार केंद्र शासति है। यानी ममता का यह कहना कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वालों पर अत्याचार होता है वह सत्य से कोसों दूर और काल्पनिक साबित होता है। अगर वाकई बंगाली बोलने वालों पर अत्याचार हो रहा होता तो संख्या कुछ और होती। अब आते हैं इसके संभावित परिणामों पर। भाषा के नाम पर खाई के संभावित परिणाम? बीते कुछ वर्षों में भारत में भाषा का प्रश्न केवल सांस्कृतिक पहचान का नहीं रह गया बल्कि कई बार यह राजनीति, क्षेत्रीय अस्मिता और सत्ता संघर्ष से जुड़कर ऐसे आंदोलनों में बदल जाता है जो हिंसा और भेदभाव का कारण बन जाता है। इसके कई उदाहरण हैं। तमिलनाडु और हिंदी-विरोध आंदोलन भाषाई राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण तमिलनाडु है। आजादी के बाद जब सरकार ने हिंदी को धीरे-धीरे राजभाषा बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए तो दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में इसका तीव्र विरोध हुआ। 1965 में जब हिंदी को राजभाषा बनाए जाने की समय-सीमा नजदीक आई तब व्यापक आंदोलन छिड़ गए। छात्रों ने आत्मदाह किए, पुलिस फायरिंग में कई लोग मारे गए। इस हिंसा ने उत्तर भारतीयों और हिंदीभाषियों के प्रति गहरी असुरक्षा और अविश्वास की भावना पैदा की। महाराष्ट्र और ‘मराठी मानुष’ की राजनीति महाराष्ट्र में भाषा और क्षेत्रीय अस्मिता का प्रश्न मुंबई और रोजगार से जुड़ा रहा। 1960 में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन ने मुंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की मांग की, जिसमें हिंसक झड़पें भी हुईं। इसके बाद शिवसेना ने ‘मराठी मानुष’ का नारा देकर पहले दक्षिण भारतीयों और फिर उत्तर भारतीय प्रवासियों को निशाना बनाया। हिंदीभाषी प्रवासियों पर हमले, दुकानों का बहिष्कार और रोजगार से बेदखली जैसी घटनाओं ने मुंबई जैसे महानगर में भाषाई भेदभाव की गहरी लकीर खींच दी। आंध्र प्रदेश और भाषाई राज्यों का पुनर्गठन भारत में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन सबसे पहले आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु ने अलग तेलुगुभाषी राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु के बाद 1953 में आंध्र राज्य का गठन हुआ। हालांकि इससे अन्य राज्यों में भी भाषाई आंदोलनों की लहर दौड़ी। आगे चलकर तेलंगाना आंदोलन में भी तेलुगुभाषी समाज के भीतर क्षेत्रीय विभाजन गहराया, जिसने हिंसा और भेदभाव को जन्म दिया। पंजाबी बनाम हिंदी का संघर्ष पंजाब में भाषा और धर्म का प्रश्न गहराई से जुड़ा रहा। 1960 के दशक में पंजाबी को आधिकारिक दर्जा दिलाने के आंदोलन ने राज्य को विभाजित कर दिया। हिंदीभाषी इलाकों को हरियाणा और हिमाचल में अलग कर दिया गया। लेकिन इस भाषाई-सांस्कृतिक विभाजन ने बाद में अलगाववाद और आतंकवाद को भी अप्रत्यक्ष रूप से हवा दी। पंजाबी बनाम हिंदी का विवाद केवल प्रशासनिक निर्णय तक नहीं रहा बल्कि सामाजिक वैमनस्य और अविश्वास का आधार और राजनीतिक हथियार बनता गया। असम और बंगाली भाषा विवाद पूर्वोत्तर भारत में भाषा का प्रश्न सबसे अधिक जटिल और हिंसक रूप में सामने आया। 1961 में असम सरकार ने असमिया को अनिवार्य करने का निर्णय लिया। इसका बंगालीभाषी समाज ने तीव्र विरोध किया। सिलचर में पुलिस गोलीबारी में 11 आंदोलनकारियों की मौत हो गई, जिसे ‘भाषा शहीद दिवस’ के रूप में याद किया जाता है। इसके बाद 1980 के दशक में असम आंदोलन ने ‘विदेशी’ के नाम पर बांग्लाभाषी समुदाय को सबसे बड़ा निशाना बनाया। बड़े पैमाने पर हिंसा और विस्थापन ने असमिया-बांग्ला समाज के बीच स्थायी खाई पैदा कर दी। कर्नाटक और तमिलनाडु का टकराव भाषा का प्रश्न कई बार जल और संसाधन विवादों से भी जुड़ता है। कावेरी जल विवाद में कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों में एक-दूसरे की भाषा बोलने वालों पर हमले हुए। दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया और आम नागरिकों को हिंसा झेलनी पड़ी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भाषा की राजनीति केवल पहचान का सवाल नहीं बल्कि क्षेत्रीय संसाधनों की लड़ाई में भी हथियार बन जाती है। भाषाई राजनीति के नकारात्मक परिणाम इन सभी घटनाओं से कुछ सामान्य नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं- हिंसा और मौतें: विभिन्न आंदोलनों में हजारों लोग मारे गए या घायल हुए। सामाजिक भेदभाव: रोज़गार, शिक्षा और व्यवसाय में ‘अपनी भाषा’ बनाम ‘दूसरी भाषा’ का भेदभाव गहराया। राजनीतिक ध्रुवीकरण: भाषाई भावनाओं पर आधारित पार्टियां मज़बूत हुईं और राष्ट्रीय एकता को चुनौती मिली। सांस्कृतिक अविश्वास: अलग-अलग भाषाभाषी समाजों के बीच स्थायी अविश्वास और दूरी बढ़ी। क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान हो राजनीति नहीं अब बात आती है कि क्या इन हिंसा को आधार मानकर क्षेत्रीय भाषाओं के अस्तित्व को नकार देना चाहिए? ऐसा कतई उचित नहीं है, न ही ऐसा कभी हो सकता है। इसके जीते-जागते उदाहरण हैं मोदी सरकार द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान और प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए ठोस कदम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है और उच्च शिक्षा व राष्ट्रीय परीक्षाओं (JEE, NEET, UGC आदि) को 12 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। AICTE ने इंजीनियरिंग शिक्षा को 11 भाषाओं में शुरू किया वहीं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ‘भाषिनी’ और DIKSHA पर लाखों कंटेंट क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। हाल ही में मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। संविधान का मैथिली में अनुवाद प्रकाशित हुआ और ‘भारतीय भाषा अनुभाग’ की स्थापना की गई। साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कार्यक्रमों और काशी-तमिल संगम जैसी पहलों से भाषाई-सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला है। इन पहलों से स्पष्ट है कि सरकार क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा, रोजगार, प्रशासन और संस्कृति के केंद्र में लाकर उन्हें केवल पहचान का प्रतीक नहीं बल्कि विकास का सशक्त माध्यम बना रही है। ‘बहुभाषी भारत’ की परिकल्पना में ही सबकी भलाई इन सभी सवालों और जवाबों से स्पष्ट होता है कि भारत की भाषाई विविधता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है लेकिन जब यही विविधता राजनीति का औजार बनती है तो यह राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन जाती है। इतिहास गवाह है कि भाषा के नाम पर चले आंदोलन कई बार अपनी मूल सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा से आगे बढ़कर हिंसा और भेदभाव का कारण बने हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि भाषा को सत्ता संघर्ष का साधन नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुल और संवाद का माध्यम बनाया जाए। संविधान ने ‘बहुभाषी भारत’ की जो परिकल्पना की थी उसे व्यवहार में लाना ही देश को भाषाई राजनीति के दुष्परिणामों से बचा सकता है।